‘पगडंडी में पहाड़’: पर्यटन से अलग, जीवन को समझने की साहित्यिक यात्रा
सचिन त्रिपाठीशोध छात्र, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ‘पगडंडी में पहाड़’ एक ऐसा यात्रा-वृत्तांत है जो उत्तराखंड के पर्वतीय जीवन, संस्कृति और पर्यावरण को गहराई से उजागर करता है। यह कृति यात्रा को केवल स्थल-वर्णन तक सीमित नहीं रखकर, जीवन के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से जोड़ती है। इसमें लोकजीवन की सूक्ष्मताओं और आध्यात्मिकता की […]
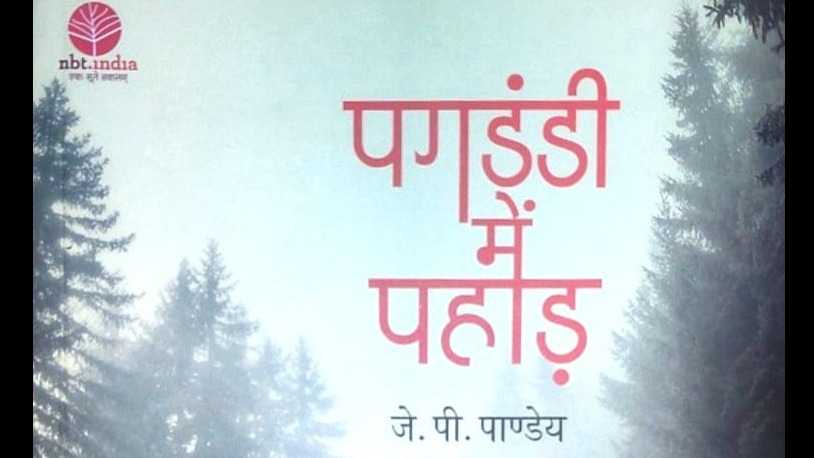
सचिन त्रिपाठी
शोध छात्र, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
‘पगडंडी में पहाड़’ एक ऐसा यात्रा-वृत्तांत है जो उत्तराखंड के पर्वतीय जीवन, संस्कृति और पर्यावरण को गहराई से उजागर करता है। यह कृति यात्रा को केवल स्थल-वर्णन तक सीमित नहीं रखकर, जीवन के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से जोड़ती है। इसमें लोकजीवन की सूक्ष्मताओं और आध्यात्मिकता की गूंज स्पष्ट रूप से महसूस होती है। इसी कृति की सूक्ष्मता और गहराई को हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय के शोध छात्र सचिन त्रिपाठी ने बड़े ही संवेदनशील और शोधपरक नजरिये से प्रस्तुत किया है।
हिंदी यात्रा-साहित्य की परंपरा में राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय, निर्मल वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी जैसे लेखकों ने यात्राओं को आत्मान्वेषण और बौद्धिक जागरण का माध्यम बनाया। इस परंपरा में पगडंडी में पहाड़ का स्थान विशिष्ट है, क्योंकि यह यात्रा को न केवल आत्मबोध, बल्कि लोकबोध, पर्यावरण-बोध और समाजबोध के स्तर तक विस्तृत करता है।

जे. पी. पाण्डेय द्वारा रचित पगडंडी में पहाड़ न केवल एक यात्रा-वृत्तांत है, बल्कि यह आधुनिक हिंदी साहित्य में उन कृतियों की पंक्ति में खड़ा होता है जो यात्रा को केवल भौगोलिक गति नहीं, बल्कि आत्मबोध की एक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करती हैं। वर्तमान हिंदी साहित्य में यात्रा-वृत्तांतों का स्थान मात्र स्थल-वर्णन या नैसर्गिक सौंदर्य की अनुभूति तक सीमित नहीं रह गया है। अब यह विधा जीवन, समाज और संस्कृति के बहुविध पक्षों को उजागर करने का माध्यम बन चुकी है।
इस कृति में लेखक ने जिस गहराई, आत्मीयता और प्रामाणिकता के साथ उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा का वृत्तांत प्रस्तुत किया है, वह निश्चय ही इसे महत्त्वपूर्ण बनाता है।
यह पुस्तक न केवल हिमालयी भूगोल का साक्षात् अनुभव कराती है, अपितु वहाँ के जनजीवन, सांस्कृतिक बुनावट और सामाजिक चेतना की गहन व्याख्या भी प्रस्तुत करती है। इस यात्रा-वृत्तांत में ‘लोक जीवन’ के स्वर इतने सूक्ष्म, यथार्थ और आत्मीय ढंग से चित्रित हुए हैं कि यह कृति लोक और शहरी पाठकों के बीच एक सेतु की भांति कार्य करती है।
यह कृति जिस प्रकार पर्वतीय क्षेत्र के जीवन के बहुआयामी पक्षों को उद्घाटित करती है, उससे स्पष्ट होता है कि लेखक ने केवल बाह्य दृष्टि से नहीं, अपितु अंतरंग संवेदना और सांस्कृतिक सहानुभूति के साथ उस जीवन को देखा, समझा और आत्मसात किया है। लोक जीवन का चित्रण यहाँ केवल सामाजिक यथार्थ का पुनरुत्पादन नहीं, बल्कि एक सजीव अनुभव-यात्रा है, जिसमें लेखक और पाठक दोनों समान रूप से सम्मिलित हो जाते हैं।
लेखक की दृष्टि केवल पर्यटक की नहीं है। वह दर्शक के रूप में नहीं, सहभागी की तरह यात्रा करता है। यही कारण है कि उसकी भाषा में पर्वतीय जीवन की कठोरता, वहाँ के जन-जीवन की गरिमा और पर्यावरण की अनुभूति सहज भाव से रच-बस गई है। यह वृत्तांत किसी योजनाबद्ध अभियान जैसा नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक बहाव है — जिसमें प्रकृति, मनुष्य, संस्कृति और अनुभूति एकसाथ प्रवाहित होती है। लेखक का यात्रा-मार्ग, उनके ठहरने और चलने की शैली, संवाद और निरीक्षण — ये सब पाठक को केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उस यात्रा में सहभागी होने के लिए आमंत्रित करते हैं।
इस पुस्तक की सबसे उल्लेखनीय विशेषता है उसकी ‘लोकगंध’। लेखक की संवेदना पर्वतीय लोक से एकात्मक संबंध स्थापित करती है। वह केवल पहाड़ नहीं देखता, बल्कि उसमें बसे जीवन को पढ़ता है। पहाड़ियों की चुप्पी में वह इतिहास की आहट सुनता है, झरनों की कल-कल में वहाँ के श्रम-संगीत को पहचानता है, और महिलाओं की पीठ पर लदे बोझ में समाज की अनकही कहानियाँ देखता है।
मसूरी की सामान्य पर्यटक-संस्कृति को छोड़कर जब लेखक झड़ीपानी, संगम फॉल, मोंसी फॉल या नाग टिब्बा जैसे स्थलों तक पहुँचता है, तब वह एक गहरे पर्यावरणीय और सामाजिक विमर्श में प्रवेश करता है। वह इन स्थलों को केवल प्राकृतिक दृश्य के रूप में नहीं, बल्कि उनके इर्द-गिर्द विकसित जीवन-शैली, संघर्ष, लोककथाओं और मान्यताओं के समुच्चय के रूप में देखता है।
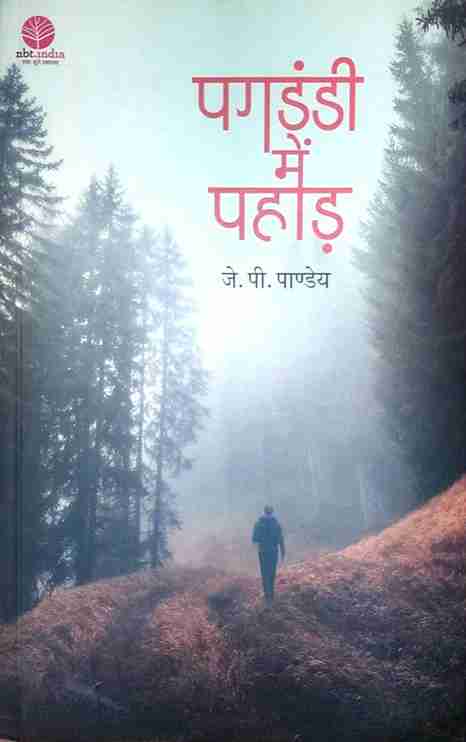
“पगडंडी में पहाड़” का शीर्षक ही अपने-आप में प्रतीकात्मक है। यह न तो किसी चौड़ी सड़क की बात करता है और न ही किसी राजसी मार्ग की। पगडंडी उस मार्ग का नाम है जो श्रमशील जन का है, जो प्रकृति से संतुलित होकर चला जाता है, जो सीधा नहीं पर सबसे सच्चा होता है। लेखक ने इस प्रतीक को संपूर्ण कृति में आत्मसात किया है।
वह किसी भी भव्य होटल, आलीशान रिसॉर्ट या पर्यटक-सुविधा का उल्लेख नहीं करता, बल्कि उन पगडंडियों से गुजरता है जहाँ ग्रामीण महिलाएँ लकड़ी लादे हुए चढ़ती हैं, बच्चे स्कूल जाते हुए पहाड़ी रास्तों पर चलते हैं और जहाँ से तीर्थों तक का श्रममूलक सफर शुरू होता है। इस कृति में धार्मिक स्थलों का वर्णन अत्यंत संयम, गरिमा और गहराई के साथ किया गया है। नाग मंदिर, बुद्ध मंदिर, भदराज मंदिर — इन सभी का उल्लेख मात्र तीर्थ-स्थलों के रूप में नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संगम और विविध आध्यात्मिक परंपराओं के सह-अस्तित्व के प्रतीक रूप में हुआ है।
लेखक इन स्थलों का चित्रण किसी चमत्कारिक या चकाचौंध भरे विवरण के बजाय सहज, अनुभवजन्य और अंतरंग भाव से करता है, जिससे पाठक को केवल स्थान-परिचय नहीं, बल्कि वहाँ की आध्यात्मिक आभा का भी आभास होता है।
नाग मंदिर और बुद्ध मंदिर का एक ही यात्रा-वृत्तांत में समावेश विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह समावेश स्पष्ट करता है कि लेखक किसी एक धार्मिक चेतना तक सीमित न रहकर, आध्यात्मिक अनुभव के बहुलतावादी और समावेशी रूप को स्वीकार करता है। एक ओर नाग मंदिर से जुड़ी हिंदू परंपरा के लोक-विश्वास और आस्था हैं, तो दूसरी ओर बुद्ध मंदिर की शांति, करुणा और ध्यान की बौद्ध दृष्टि है। लेखक इन दोनों को विरोधी ध्रुवों के रूप में नहीं, बल्कि एक ही पर्वतीय जीवन-धारा के अभिन्न अंग के रूप में देखता है।
अंतिम खंडों में प्रमुख पर्यटन स्थलों के साथ-साथ प्रसिद्ध चारधाम यात्रा, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी के बारे में भी आकर्षक जानकारी दी गई है। गंगोत्री का वर्णन लेखक की गहरी आध्यात्मिक संवेदना का उदाहरण है —
“गंगोत्री का दृश्य अविस्मरणीय था। माँ गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से अवतरित होती हैं। इस पवित्र स्थान पर खड़े होकर मैं अत्यंत रोमांचित था। घाट के किनारे पड़ी एक बेंच पर एकांत में बैठकर मैं घंटों प्राकृतिक दृश्य के रूप में उस परम शक्ति से एकाकार होता रहा।”
यह उद्धरण स्पष्ट करता है कि लेखक के लिए धार्मिक स्थल केवल आस्था-केन्द्र नहीं, बल्कि आत्म-मनन और प्रकृति के साथ आध्यात्मिक एकत्व के स्थान भी हैं।
यहाँ धर्म किसी विभाजन की रेखा नहीं खींचता, बल्कि सह-अस्तित्व की वह धरातल तैयार करता है, जिस पर भिन्न परंपराएँ, विश्वास और पूजा-पद्धतियाँ एक-दूसरे के साथ फलती-फूलती हैं। लेखक की यह दृष्टि पाठक को यह संदेश देती है कि भारत की शक्ति उसकी विविधता में निहित है, और यह विविधता तब तक जीवंत है जब तक उसमें स्वीकार्यता, संवाद और सम्मान की भावना बनी रहे।
मसूरी के पार घट्टा पानी या चायख़ान जैसी यात्राओं में लेखक उस सांस्कृतिक भूगोल को उकेरते हैं जो न तो औपचारिक इतिहास में सुरक्षित है और न ही पर्यटन-ब्रोशर में दर्ज। यहाँ का जल, हवा, शोर, चुप्पी और संवाद — सब कुछ पाठक के लिए एक जीवंत अनुभव बन जाता है।
“हेमकुंड साहेब एवं फूलों की घाटी” अध्याय में लेखक केवल स्थल का सौंदर्य नहीं वर्णित करता, बल्कि उसे आस्था, श्रम और सामूहिक तीर्थ-चेतना के रूप में प्रस्तुत करता है। लेखक के पास ‘दृश्य’ को ‘भाव’ में बदलने की एक दुर्लभ क्षमता है, जो इस कृति को साहित्यिक ऊँचाई प्रदान करती है।

1. पर्यावरणीय चेतना: प्रकृति से मैत्री का दृष्टिकोण
लेखक की यात्रा-दृष्टि में एक गहरा पर्यावरणीय संवेदन निहित है। यह संवेदन किसी अकादमिक विमर्श या औपचारिक विचारधारा का प्रतिफल नहीं, बल्कि वर्षों के सजीव अनुभवों और देखे-भोगे परिवेश की देन है।
“मसूरी के पार घट्टा पानी” या “फूलों की घाटी” जैसे अध्यायों में जब लेखक जल-स्रोतों की निर्मल धारा, विविध रंगों से सजी वनस्पति, चट्टानों पर बहते झरनों और दूर तक फैली पर्वत-श्रेणियों का वर्णन करता है, तब वह केवल प्राकृतिक दृश्यांकन नहीं करता, बल्कि इन सबके भीतर छिपे संकट, हो रहे परिवर्तनों और मनुष्य के हस्तक्षेप को भी बारीकी से रेखांकित करता है।
लेखक की यह पर्यावरणीय दृष्टि कहीं भी आरोपित या बनावटी नहीं लगती; वह इसे बिना किसी आदर्शवादी उपदेश या भाषण के, सहज अनुभूति के रूप में प्रस्तुत करता है।
उदाहरणस्वरूप, जब वह गाँवों में प्लास्टिक के कचरे का फैलाव या सूखती हुई जलधाराओं की पीड़ा का उल्लेख करता है, तब उसमें एक संवेदनशील यात्री की बेचैनी और असहायता स्पष्ट झलकती है। यह पीड़ा केवल प्रकृति की क्षति पर नहीं, बल्कि उस मानवीय असंवेदनशीलता पर भी है, जो अपने ही जीवन-स्रोत को नष्ट करती जा रही है।
आज के समय में, जब पर्यटन और तथाकथित विकास के नाम पर प्रकृति को मात्र उपभोग की वस्तु मान लिया गया है, यह दृष्टिकोण अत्यंत प्रासंगिक और आवश्यक है। जे. पी. पाण्डेय का वृत्तांत इस प्रवृत्ति का प्रतिरोध करता है और पाठक को यह स्मरण कराता है कि प्रकृति से मैत्री, सह-अस्तित्व और संरक्षण — केवल नैतिक आदर्श नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की मूल शर्त हैं।
2. लोक भाषा और बोली का आत्मीय उपयोग
“पगडंडी में पहाड़” में वर्णित लोक जीवन का एक अत्यंत प्रभावशाली और विशिष्ट पक्ष वहाँ की बोली और भाषा है। लेखक ने जिस आत्मीयता और संवेदनशीलता के साथ स्थानीय शब्दों, कहावतों और लोकोक्तियों को अपनी अभिव्यक्ति में पिरोया है, वह केवल भाषिक अलंकरण या शब्द-सज्जा नहीं है, बल्कि उस समाज की संज्ञा-प्रणाली और मानसिकता का गहरा बोध कराता है।
इन शब्दों के माध्यम से पाठक केवल वर्णन सुनता नहीं, बल्कि उस क्षेत्रीय संस्कृति को जीने, महसूस करने और समझने लगता है।
पर्वतीय भाषिक परिवेश में प्रयुक्त शब्द, जैसे कि “चश्मा” — जो यहाँ शुद्ध, स्वच्छ और प्राकृतिक जलस्रोत के लिए प्रयुक्त होता है — केवल भौगोलिक तत्व का परिचय नहीं देते, बल्कि वे वहाँ के लोगों की प्रकृति-निष्ठ जीवन-दृष्टि को भी उजागर करते हैं।
इसी तरह अन्य स्थानीय संज्ञाएँ, खेती-बाड़ी के उपकरणों, वनस्पतियों, ऋतु-परिवर्तन और त्योहारों के लिए प्रयुक्त विशिष्ट शब्द — उस लोक-समाज के अनुभव-संसार को भाषा में मूर्त रूप देते हैं।
लेखक की लेखनी में बोली की सहजता और उसमें अंतर्निहित अनुभूतियाँ पर्वतीय लोकजीवन की जीवंतता और आत्मीयता को रेखांकित करती हैं। इस तरह भाषा और बोली केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कृति, इतिहास और सामाजिक स्मृति की वाहक बनकर उभरती हैं।
3. स्थानों के इतिहास और विस्तृत जानकारी का संयमित प्रस्तुतीकरण
“पगडंडी में पहाड़” की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें वर्णित प्रत्येक स्थल के साथ उसका इतिहास, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और स्थानीय जानकारी भी विस्तार से प्रस्तुत की गई है। लेखक केवल दृश्य का वर्णन भर नहीं करता, बल्कि उस स्थान की ऐतिहासिक परतों को खोलता है, वहाँ से जुड़े लोक-विश्वास, घटनाएँ और व्यक्तित्वों का भी उल्लेख करता है।
इससे पाठक को न केवल यात्रा का अनुभव मिलता है, बल्कि उस स्थान की सांस्कृतिक स्मृति और ऐतिहासिक महत्व का भी बोध होता है। उदाहरण के लिए, लेखक जब उत्तराखंड का विवरण करते हैं, तब वे इस स्थान के इतिहास का विस्तृत चित्र प्रस्तुत करते हैं:
“सातवीं शताब्दी से ग्यारहवीं शताब्दी तक यहाँ कटपुरी शासकों ने शासन किया। वासुदेव कटपुरी ने इस राजवंश की स्थापना की और कार्तिकेयपुर (अब बैजनाथ) इस राजवंश की राजधानी थी।
अपने गौरव के चरम पर इस राजवंश ने नेपाल से लेकर अफगानिस्तान तक शासन किया। नेपाल के कंचनपुर जिले में ब्रह्मदेव नामक कटपुरी शासक ने ब्रह्मदेव मंडी की स्थापना की थी।
12वीं शताब्दी में यह राजवंश विघटित हो गया और चंद शासकों ने इस क्षेत्र पर शासन किया। 1581 में रूपचंद्र नामक राजा ने संपूर्ण कुमाऊँ क्षेत्र पर पुनः शासन स्थापित किया। 13वीं-14वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर आठ विभिन्न राजवंशों ने शासन किया।
चंद राजाओं ने चंपावत को अपनी राजधानी बनाया और बाज बहादुर इस राजवंश के सबसे प्रभावशाली राजा हुए।”
इस प्रकार, यात्रा-वृत्तांत एक सामान्य मार्गदर्शिका से कहीं आगे जाकर इतिहास, भूगोल, लोककथा और व्यक्तिगत अनुभव का संगम बन जाता है। यही गुण इसे मात्र पर्यटक-नोट्स से अलग कर, एक ऐसी साहित्यिक कृति में बदल देता है, जो पढ़ने वाले के मन में स्थलों के प्रति गहरी स्मृति और सम्मान छोड़ जाती है।
4. आर्थिक जीवन और श्रम की संस्कृति
पर्वतीय लोक जीवन का एक अनिवार्य एवं अपरिहार्य पक्ष उसकी विशिष्ट श्रम-संस्कृति है। यहाँ के कठोर, ऊबड़-खाबड़ और अनेक बार चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों में जीवन-निर्वाह का एकमात्र विश्वसनीय साधन श्रम ही है।
लेखक ने अपने यात्रा-वृत्तांत में बड़े ही सजीव और आत्मीय ढंग से खेतों की सीढ़ीदार व्यवस्था, पशुपालन की परंपरा, मौसमी फसलों की विविधता तथा पर्वतीय कारीगरी के अनुपम कौशल का वर्णन किया है। इन विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ का जीवन केवल संघर्ष और कठिनाई का पर्याय नहीं है, बल्कि श्रम को सौंदर्य, गरिमा और सामुदायिक गौरव से जोड़कर देखने की एक गहरी परंपरा भी है।
पर्वतीय अंचलों में कृषि और पशुपालन न केवल आजीविका का आधार हैं, बल्कि यह लोगों के सामूहिक जीवन की धुरी भी हैं। सीढ़ीदार खेतों में सामूहिक रूप से बुवाई और कटाई का कार्य, पहाड़ी नालों से पानी लाकर सिंचाई करना, और मौसम के अनुसार फसलों का चुनाव — ये सब एक तरह से जीवन की लय और ऋतुचक्र के साथ सामंजस्य का प्रतीक हैं।
यहाँ श्रम केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि पर्व और अनुष्ठान का हिस्सा भी है। खेतों में काम करते समय गाए जाने वाले लोकगीत, सामूहिक श्रम के अवसरों पर आपसी हँसी-मजाक और पारंपरिक उत्सव — श्रम को थकान नहीं, बल्कि आनंद और सामाजिक मेल-जोल में बदल देते हैं।
इस प्रकार, पर्वतीय लोक का आर्थिक जीवन केवल जीविका अर्जन का यांत्रिक प्रयास नहीं है, बल्कि यह श्रम, सौंदर्य-बोध और सामुदायिक जीवन की एक ऐसी सजीव परंपरा है, जिसमें कठिन परिस्थितियों के बीच भी मनुष्य अपनी रचनात्मकता और सहकारिता से जीवन को गरिमा और उल्लास से भर देता है।
5. लोक-विश्वास और प्रकृति के प्रति सहअस्तित्व की भावना
लोक जीवन का एक प्रमुख आधार उसका प्रकृति से गहरा तादात्म्य है। “पगडंडी में पहाड़” में पर्वतीय जनमानस की यह भावना बार-बार उभरकर आती है कि प्रकृति केवल संसाधन नहीं, बल्कि एक जीवंत सत्ता है, जिसके साथ उनका संबंध मात्र उपयोग का नहीं, बल्कि संवेदनात्मक जुड़ाव का है।
गाँव के आसपास फैले जंगल, पगडंडियों से जुड़ी पहाड़ी ढलानें, नीलाभ आकाश के नीचे फैली पर्वत-श्रृंखलाएँ और कल-कल बहते जलस्रोत — ये सब केवल भौगोलिक संरचनाएँ नहीं, बल्कि मानो परिवार के सदस्य हों, जिनके सुख-दुःख में मनुष्य स्वयं को सहभागी समझता है।
पर्वतीय समाज में यह धारणा गहरी जड़ें जमाए हुए है कि जंगल, जल और जमीन का संरक्षण ही जीवन का संरक्षण है। गाँव की पगडंडी हो या पहाड़ की चोटी, सबका एक जीवन-चरित्र है और वह समुदाय के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है।
यही सहअस्तित्व का भाव उन्हें पेड़ों की छाँव, पहाड़ी चश्मों के जल और जंगल की छुपी पगडंडियों के प्रति गहरा आदरभाव देता है।
लेखक ने अपने यात्रा-वृत्तांत में न केवल इस परंपरागत पर्यावरणीय चेतना को रेखांकित किया है, बल्कि आधुनिक विकास की अंधी दौड़ से उपजे संकटों को भी सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से उजागर किया है।
एक स्थान पर वे जंगल के जल जाने का दृश्य वर्णित करते हैं — पेड़ों की जली हुई शाखाएँ और निःशब्द खड़े वृक्ष, जैसे अपनी पीड़ा कहने में असमर्थ हों। लेखक को यह दृश्य भीतर तक उद्वेलित कर देता है, मानो उन्होंने किसी जीवंत मित्र को खो दिया हो। यह प्रसंग पाठक को झकझोरता है और यह समझने पर विवश करता है कि प्रकृति का विनाश, वस्तुतः हमारे अपने अस्तित्व पर आघात है।
समाप्ति: एक संवादधर्मी सांस्कृतिक-पाठ
इस प्रकार “पगडंडी में पहाड़” केवल प्रकृति की रमणीयता का चित्रण भर नहीं करता, बल्कि उस सहजीवन-भावना को भी प्रकट करता है, जिसमें मनुष्य और प्रकृति एक-दूसरे के संरक्षक, संवाहक और सहयात्री बनकर जीते हैं।
“पगडंडी में पहाड़” यात्रा-वृत्तांत मात्र स्थानिक अनुभवों की कथा नहीं है, यह लोक जीवन की अदृश्य धड़कनों को रेखांकित करने वाला एक सांस्कृतिक-पाठ है।
इसमें लोक केवल वर्ण्य विषय नहीं, बल्कि वह दृष्टिकोण है जिससे लेखक ने जीवन को देखा है। यह कृति न केवल एक पर्वतीय प्रदेश के जनजीवन को सामने लाती है, बल्कि उसकी आत्मा, उसकी भाषा, उसकी श्रद्धा और उसके संघर्ष को भी पाठकों तक पहुँचाती है।
लोक जीवन के इस अद्भुत चित्रण के माध्यम से प्रियंवद न केवल एक लेखक, बल्कि लोक का संवाहक बनकर उभरते हैं।
यह कृति यात्रा-साहित्य में एक नया मुहावरा गढ़ती है — जिसमें न तो दिखावटी रोमांच है, न ही आत्मकेंद्रित लेखकीय प्रदर्शन; बल्कि इसमें एक सतत संवाद है — लेखक, स्थान, समाज और पाठक के बीच।
यही संवादात्मकता इस कृति को शोध, शिक्षण और पाठकीय आनंद — तीनों ही स्तरों पर मूल्यवान बनाती है।
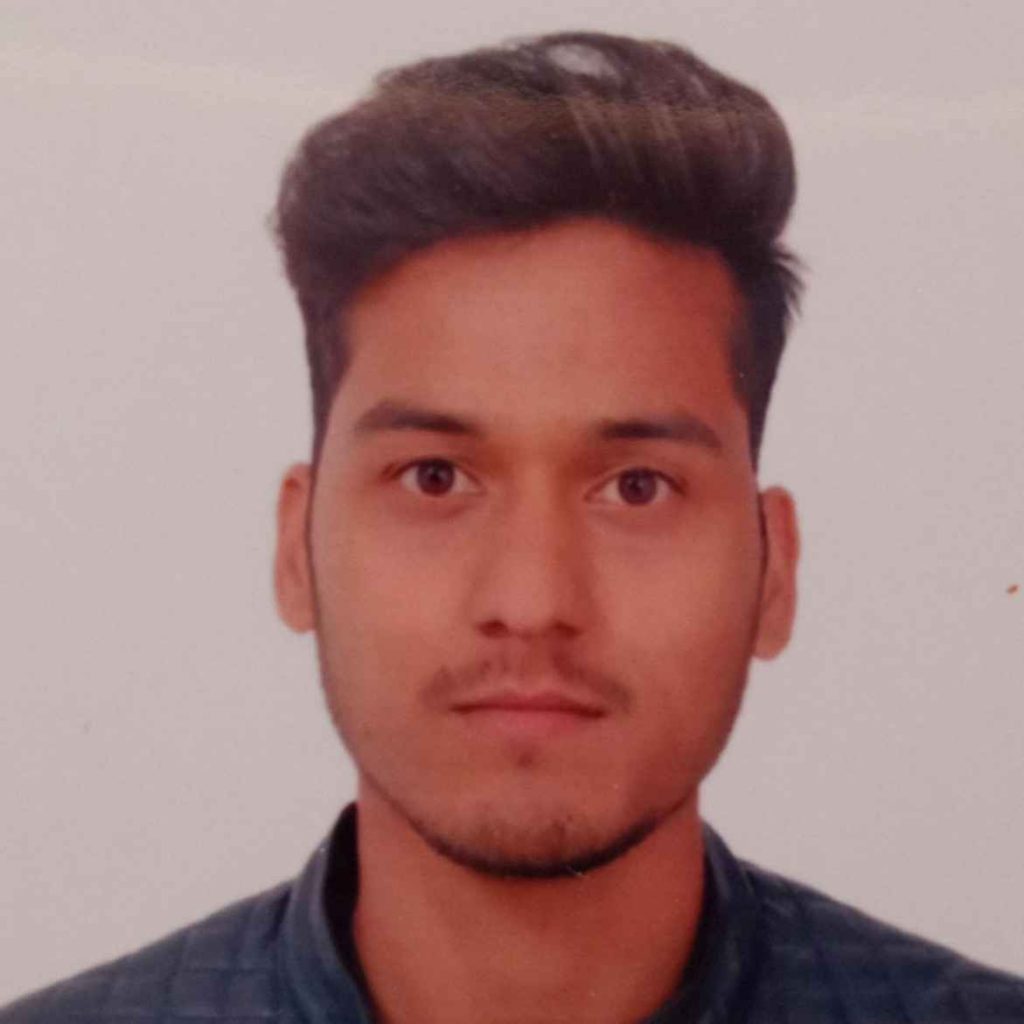
लेखक सचिन त्रिपाठी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में शोध छात्र हैं। वे हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में गहन अध्ययन एवं शोध कार्य कर रहे हैं। उनके शोध का प्रमुख क्षेत्र समकालीन हिंदी साहित्य और आलोचना है।









